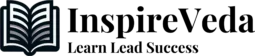प्राचीन भारत (Ancient India)
वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विकास
भारत की सामाजिक संरचना में वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह व्यवस्था आरंभ में कर्म आधारित थी, लेकिन समय के साथ यह जन्म आधारित जाति प्रथा में बदल गई। इस लेख में हम इस सामाजिक व्यवस्था के विकास को समझेंगे।
1. वर्ण व्यवस्था का उद्भव
- ऋग्वेद में समाज को चार वर्णों में बाँटा गया — ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
- यह विभाजन मुख्यतः कार्य और गुण पर आधारित था।
- पुरुषसूक्त (ऋग्वेद) में इस वर्ण विभाजन का उल्लेख मिलता है।
2. चार वर्णों के कार्य
| वर्ण | मुख्य कार्य |
|---|---|
| ब्राह्मण | शिक्षा, यज्ञ, धर्म का प्रचार |
| क्षत्रिय | रक्षा, शासन, युद्ध |
| वैश्य | कृषि, व्यापार, पशुपालन |
| शूद्र | सेवा कार्य, अन्य वर्णों की सहायता |
3. जाति प्रथा का विकास
- उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित बन गई।
- जातियाँ अनेक उपवर्णों में विभाजित हो गईं जिन्हें ‘जाती’ कहा जाने लगा।
- जाति व्यवस्था में उच्च और निम्न की अवधारणा विकसित हुई।
- सामाजिक गतिशीलता सीमित हो गई और छुआछूत जैसी कुप्रथाएं उत्पन्न हुईं।
4. सामाजिक प्रभाव
- सामाजिक विषमता और भेदभाव की जड़ें मजबूत हुईं।
- समाज में ऊँच-नीच का भाव गहराया।
- बौद्ध और जैन धर्म ने इस व्यवस्था की आलोचना की।
- आधुनिक भारत में इस व्यवस्था के विरुद्ध कई सुधार आंदोलन हुए।
5. जाति प्रथा के विरुद्ध सुधार आंदोलन
- राजा राम मोहन राय – ब्राह्म समाज
- ज्योतिबा फुले – सत्यशोधक समाज
- डॉ. भीमराव अंबेडकर – दलित आंदोलन, जाति उन्मूलन
- स्वामी दयानंद सरस्वती – आर्य समाज
आश्रम व्यवस्था एवं पुरोहित वर्ग की भूमिका
प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था में आश्रम व्यवस्था और पुरोहित वर्ग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आश्रम जीवन के चार चरणों को दर्शाता है जबकि पुरोहित वर्ग धार्मिक एवं सामाजिक दिशा देने में अग्रणी भूमिका निभाता था।
1. आश्रम व्यवस्था का परिचय
आश्रम व्यवस्था वैदिक काल में विकसित एक सामाजिक प्रणाली थी, जिसमें जीवन को चार चरणों में बाँटा गया:
| आश्रम | आयु सीमा | मुख्य उद्देश्य |
|---|---|---|
| ब्रह्मचर्य आश्रम | 0-25 वर्ष | विद्या अध्ययन, गुरुसेवा, संयम |
| गृहस्थ आश्रम | 25-50 वर्ष | परिवार, सामाजिक दायित्व, धर्म पालन |
| वानप्रस्थ आश्रम | 50-75 वर्ष | वैराग्य, ध्यान, समाज सेवा |
| संन्यास आश्रम | 75 वर्ष के बाद | मोक्ष की ओर प्रयाण, त्याग |
2. आश्रम व्यवस्था के लाभ
- व्यक्तिगत और सामाजिक संतुलन बना रहता था।
- हर आश्रम में नैतिक और सामाजिक कर्तव्य निर्धारित होते थे।
- धार्मिकता, परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना का विकास होता था।
3. पुरोहित वर्ग की भूमिका
- ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग धर्म, वेदों, यज्ञ और संस्कार में निपुण होता था।
- राजा के सलाहकार, शिक्षक और यज्ञ के संचालनकर्ता होते थे।
- सामाजिक मर्यादा, शिक्षा और धार्मिक अनुशासन को बनाए रखते थे।
- धर्म ग्रंथों की व्याख्या और नियमों की संरचना में अग्रणी रहते थे।
4. आलोचना और परिवर्तन
- समय के साथ पुरोहित वर्ग में आडंबर और कट्टरता आ गई।
- जातिवाद और सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा मिला।
- बौद्ध एवं जैन धर्म ने पुरोहितवाद की आलोचना की और सरल धर्म का मार्ग बताया।
5. निष्कर्ष
आश्रम व्यवस्था एक सुव्यवस्थित जीवन प्रणाली थी जिसने व्यक्ति को धर्म, कर्तव्य और आत्मविकास के पथ पर चलने हेतु प्रेरित किया। वहीं पुरोहित वर्ग ने समाज को धार्मिक और सांस्कृतिक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यद्यपि बाद में उसमें विकृतियाँ भी आईं।
स्त्रियों की स्थिति (वैदिक और उत्तर वैदिक काल में)
भारतीय इतिहास में स्त्रियों की सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती रही है। वैदिक काल में महिलाओं को उच्च सम्मान प्राप्त था, जबकि उत्तर वैदिक काल में उनका स्थान धीरे-धीरे नीचे गिरता गया।
1. वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति
- स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता थी।
- स्त्रियाँ वेदों का अध्ययन करती थीं और यज्ञों में भाग लेती थीं।
- उनका विवाह प्रायः विवाह योग्य आयु के बाद होता था।
- पति के साथ समान धार्मिक कर्तव्यों में सहभागिता रहती थी।
- प्रसिद्ध ऋषिकाएं: घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, आदि।
2. उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति
- स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई।
- शिक्षा का अधिकार सीमित हो गया।
- बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा की शुरुआत हुई।
- स्त्रियाँ धार्मिक अनुष्ठानों से दूर कर दी गईं।
- उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता था।
3. तुलना सारणी
| पहलू | वैदिक काल | उत्तर वैदिक काल |
|---|---|---|
| शिक्षा | सुलभ एवं सम्मानजनक | सीमित या प्रतिबंधित |
| विवाह | स्वयंवर प्रणाली, देर से विवाह | बाल विवाह प्रचलित |
| धार्मिक अधिकार | यज्ञ व वेद अध्ययन में भागीदारी | धार्मिक गतिविधियों से दूर |
| सामाजिक स्थिति | समानता व सम्मान | हीनता और निर्भरता |
4. निष्कर्ष
वैदिक काल में स्त्रियाँ ज्ञान, धर्म और समाज में सक्रिय भूमिका निभाती थीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संरचना में आए परिवर्तन और कर्मकांड की बढ़ती जटिलता के कारण उनकी स्थिति कमजोर हो गई।
धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं – वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ
प्राचीन भारतीय सभ्यता की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं मुख्यतः वैदिक साहित्य पर आधारित थीं। वेद, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथों ने धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक विचारों को दिशा दी। इन ग्रंथों में न केवल ईश्वर और आत्मा की अवधारणा मिलती है, बल्कि यज्ञ, कर्म और मोक्ष जैसे विचार भी वर्णित हैं।
1. वेद (Vedas)
- वेद चार हैं – ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
- ऋग्वेद: सबसे प्राचीन, देवताओं की स्तुतियों का संकलन।
- यजुर्वेद: यज्ञों से संबंधित मंत्र।
- सामवेद: गायन के लिए रचित मंत्र।
- अथर्ववेद: जादू-टोना, औषधि और गृहस्थ जीवन से संबंधित ज्ञान।
| वेद | मुख्य विषय |
|---|---|
| ऋग्वेद | स्तुतियाँ व देवताओं की आराधना |
| यजुर्वेद | यज्ञ अनुष्ठान |
| सामवेद | गायन एवं संगीत |
| अथर्ववेद | जादू-टोना, औषधि, घरेलू विधियाँ |
2. ब्राह्मण ग्रंथ
- वेदों की व्याख्या करने वाले गद्यात्मक ग्रंथ हैं।
- यज्ञ की विधियों, कर्मकांडों और धार्मिक परंपराओं का विवरण मिलता है।
- प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ: ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण।
- ब्राह्मण ग्रंथों से पुरोहित वर्ग की भूमिका और धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व स्पष्ट होता है।
3. उपनिषद
- दर्शन और आत्मज्ञान पर केंद्रित ग्रंथ हैं।
- ‘उपनिषद’ का अर्थ है – गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना।
- कर्मकांड के स्थान पर ज्ञान, आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष जैसे विचार प्रमुख हैं।
- प्रसिद्ध उपनिषद: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, माण्डूक्य, छांदोग्य, बृहदारण्यक आदि।
4. तुलना तालिका
| ग्रंथ | स्वरूप | मुख्य विषय |
|---|---|---|
| वेद | मंत्र, सूक्त | देव आराधना, यज्ञ |
| ब्राह्मण | गद्य | कर्मकांड, यज्ञ विधि |
| उपनिषद | दार्शनिक गद्य | आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष |
5. निष्कर्ष
वेद, ब्राह्मण और उपनिषद न केवल धार्मिक ग्रंथ हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति की गहराई और विचारशीलता का प्रमाण भी हैं। जहाँ वेदों ने कर्म और भक्ति का मार्ग दिखाया, वहीं उपनिषदों ने ज्ञान और आत्मविकास पर बल दिया।
बौद्ध और जैन धर्म के सामाजिक प्रभाव
बौद्ध और जैन धर्म भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के प्रमुख कारक रहे हैं। इन दोनों धर्मों ने वैदिक ब्राह्मणवादी परंपरा को चुनौती दी और समाज को नैतिक, अहिंसात्मक और सरल जीवन के सिद्धांतों की ओर प्रेरित किया।
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| वर्ण व्यवस्था की आलोचना | बौद्ध और जैन धर्म ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया और कर्म आधारित समाज की बात की। |
| अहिंसा का प्रचार | इन धर्मों ने हिंसा का विरोध किया, जिससे पशु बलि की परंपरा में गिरावट आई। |
| स्त्रियों की भागीदारी | इन धर्मों में महिलाओं को संघ (संघ की सदस्यता) में स्थान मिला, विशेष रूप से बौद्ध भिक्षुणी परंपरा में। |
| साधु-संन्यास की परंपरा | जैन और बौद्ध दोनों धर्मों में संयम, तपस्या और त्याग को सामाजिक आदर्श बनाया गया। |
| धर्म के प्रचार में जनभाषा का प्रयोग | संस्कृत की बजाय पाली और प्राकृत जैसी जनभाषाओं का प्रयोग कर आम जनता को जोड़ने का प्रयास किया गया। |
| शिक्षा और मठ-व्यवस्था | बौद्ध मठ जैसे नालंदा, विक्रमशिला आदि शिक्षा के प्रमुख केंद्र बने, जिससे समाज में ज्ञान का प्रसार हुआ। |
शिक्षा प्रणाली – गुरुकुल, तक्षशिला, नालंदा आदि
प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली न केवल ज्ञान का संचार करती थी बल्कि जीवन के नैतिक मूल्यों को भी विकसित करती थी। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को चारों आश्रमों के अनुसार समाजोपयोगी बनाना था।
गुरुकुल प्रणाली
- शिक्षा गुरु के आश्रम (गुरुकुल) में दी जाती थी।
- गुरु और शिष्य का संबंध पारिवारिक होता था।
- शिक्षा निःशुल्क होती थी लेकिन गुरुदक्षिणा अनिवार्य होती थी।
- विषयों में वेद, व्याकरण, गणित, खगोलशास्त्र, संगीत आदि सम्मिलित थे।
तक्षशिला विश्वविद्यालय
- यह विश्व का प्रथम ज्ञात विश्वविद्यालय माना जाता है।
- स्थापना 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुई थी।
- यह वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित था।
- प्रसिद्ध शिक्षक – आचार्य चाणक्य, चरक, जीवक।
- प्रमुख विषय – चिकित्सा, आयुर्वेद, राजनीति, सैन्य विज्ञान।
नालंदा विश्वविद्यालय
- स्थापना गुप्त वंश के शासनकाल में (5वीं शताब्दी ई.) हुई।
- यह बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित था।
- ह्वेनसांग ने इसकी अत्यधिक प्रशंसा की है।
- यहां हजारों छात्र और शिक्षक विद्यमान रहते थे।
- प्रमुख विषय – बौद्ध दर्शन, व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा।
प्राचीन शिक्षा प्रणाली की विशेषताएँ
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| नैतिक शिक्षा | सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य जैसे मूल्यों पर बल। |
| आध्यात्मिक दृष्टिकोण | वेदों, उपनिषदों, योग और ध्यान की शिक्षा। |
| समावेशिता | सभी वर्णों को शिक्षा का अधिकार (प्रारंभिक वैदिक काल में)। |
पारिवारिक संरचना और विवाह प्रथा (सामाजिक आचार-विचार)
पारिवारिक संरचना भारतीय समाज की आधारभूत इकाई रही है। वैदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक परिवार समाज का केन्द्र रहा।
- पिता को परिवार का मुखिया माना जाता था।
- संतानों की परवरिश, शिक्षा और विवाह की जिम्मेदारी पिता की होती थी।
- आर्थिक गतिविधियाँ, यज्ञ, धार्मिक कार्य आदि सामूहिक रूप से परिवार में संपन्न होते थे।
- संपत्ति के अधिकारों के कारण संयुक्त परिवार कमजोर हुए।
- उत्तराधिकार प्रणाली में पुत्र को वरीयता दी जाने लगी।
विवाह प्रथा भारतीय समाज में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों से जुड़ी हुई रही है।
- कन्या को वर चुनने की स्वतंत्रता (स्वयंवर) प्राप्त थी।
- एकपत्नी प्रथा प्रचलित थी, हालांकि राजाओं में एकाधिक विवाह भी पाए जाते थे।
- ब्राह्म विवाह को श्रेष्ठ माना गया (वर को दान में कन्या देना)।
- बाल विवाह, दहेज प्रथा की शुरुआत हुई।
- सामाजिक स्थिति और वर्ण व्यवस्था के अनुसार विवाह सीमित हुए।
- अंतरवर्णीय विवाह को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली।
सामाजिक आचार-विचार
- सामाजिक जीवन धार्मिक परंपराओं से प्रभावित था।
- पुरुषों के लिए शिक्षा और यज्ञ अनिवार्य माने जाते थे।
- स्त्रियाँ सीमित अधिकारों के साथ जीवन जीती थीं, विशेषकर उत्तर वैदिक काल में।
- गुरु, ब्राह्मण, अतिथि और माता-पिता का विशेष सम्मान किया जाता था।
श्रमिक वर्ग और दास प्रथा
प्राचीन भारतीय समाज में सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा श्रमिक वर्ग और दास प्रथा से जुड़ा था। यह व्यवस्था सामाजिक असमानता और वर्ग विभाजन को दर्शाती थी, जिसमें कुछ वर्गों को सेवा और परिश्रम के कार्यों के लिए नियत किया गया था।
श्रमिक वर्ग को “शूद्र” और दासों को “दास” या “दासी” कहा जाता था। इन्हें समाज की सबसे निचली सीढ़ी पर रखा गया था।
श्रमिक वर्ग की स्थिति
- वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को श्रम कार्यों के लिए नियुक्त किया गया था।
- ये लोग कृषि, निर्माण, सेवा और अन्य शारीरिक श्रम वाले कार्य करते थे।
- उच्च वर्ण के लोगों द्वारा इन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था।
दास प्रथा का स्वरूप
- दास प्रथा वैदिक काल से ही प्रचलन में थी।
- दास और दासियाँ उच्च वर्ग के लोगों के घरों में सेवक के रूप में काम करते थे।
- कुछ दास युद्ध में पकड़े गए, तो कुछ ऋण के कारण दास बन जाते थे।
- बौद्ध और जैन धर्म ने दास प्रथा का विरोध किया।
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| शूद्र | समाज के सबसे निचले वर्ग, जो श्रम कार्यों से जुड़े थे। |
| दास | स्वतंत्रता से वंचित, मालिक के अधीन सेवक या मजदूर। |
| प्रभाव | सामाजिक असमानता और वर्गीय भेदभाव को बढ़ावा मिला। |
महत्वपूर्ण बिंदु
- दासों की स्थिति अमानवीय थी, परंतु कुछ मामलों में उन्हें रिहा भी किया जा सकता था।
- बौद्ध और जैन धर्म के उदय से दास प्रथा को नैतिक रूप से चुनौती मिली।
- समय के साथ दास प्रथा में बदलाव आया और कुछ दासों को शिक्षा और स्वतंत्रता भी मिली।
श्रमिक वर्ग और दास प्रथा प्राचीन समाज की सामाजिक संरचना में गहराई से जुड़ी थी, जो आज के सामाजिक न्याय और समानता की अवधारणाओं के विपरीत थी।
- ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे?
a) इन्द्र
b) शिव
c) विष्णु
d) ब्रह्मा
उत्तर: a) इन्द्र - वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता था?
a) पाठशाला
b) विश्वविद्यालय
c) गुरुकुल
d) ज्ञानपीठ
उत्तर: c) गुरुकुल - नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था?
a) मौर्य काल
b) गुप्त काल
c) सैन्य काल
d) हर्षवर्धन काल
उत्तर: d) हर्षवर्धन काल - बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे?
a) महावीर
b) चाणक्य
c) गौतम बुद्ध
d) नागार्जुन
उत्तर: c) गौतम बुद्ध - जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे?
a) ऋषभदेव
b) पार्श्वनाथ
c) महावीर स्वामी
d) नमिनाथ
उत्तर: c) महावीर स्वामी - वेदों की संख्या कितनी है?
a) दो
b) तीन
c) चार
d) छह
उत्तर: c) चार - उपनिषद मुख्यतः किस विषय से संबंधित हैं?
a) काव्य
b) नाट्य
c) दर्शन
d) व्याकरण
उत्तर: c) दर्शन - ‘चरैवेति चरैवेति’ वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है?
a) उपनिषद
b) ऋग्वेद
c) महाभारत
d) ब्राह्मण ग्रंथ
उत्तर: b) ऋग्वेद - ऋग्वैदिक काल में समाज का प्रमुख आधार क्या था?
a) कृषि
b) व्यापार
c) पशुपालन
d) दस्तकारी
उत्तर: c) पशुपालन - ब्राह्मण ग्रंथ किसके पूरक माने जाते हैं?
a) वेद
b) उपनिषद
c) पुराण
d) स्मृति
उत्तर: a) वेद - तक्षशिला विश्वविद्यालय किस क्षेत्र में स्थित था?
a) बिहार
b) कश्मीर
c) पंजाब (अब पाकिस्तान में)
d) गुजरात
उत्तर: c) पंजाब (अब पाकिस्तान में) - बौद्ध धर्म की भाषा कौन-सी थी?
a) संस्कृत
b) पाली
c) प्राकृत
d) मगधी
उत्तर: b) पाली - वैदिक काल में स्त्रियों को कौन-सा अधिकार प्राप्त था?
a) युद्ध
b) राजनीति
c) यज्ञ में भागीदारी
d) शिक्षा पर रोक
उत्तर: c) यज्ञ में भागीदारी - अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे?
a) देवनागरी
b) ब्राह्मी
c) खरोष्ठी
d) पाली
उत्तर: b) ब्राह्मी - महाजनपदों की संख्या कितनी थी?
a) 12
b) 16
c) 20
d) 24
उत्तर: b) 16 - दास प्रथा का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है?
a) मनुस्मृति
b) महाभारत
c) ऋग्वेद
d) अर्थशास्त्र
उत्तर: c) ऋग्वेद - महाभारत को किसने रचा?
a) वाल्मीकि
b) वेदव्यास
c) पतंजलि
d) भास
उत्तर: b) वेदव्यास - गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है?
a) बौद्ध युग
b) स्वर्ण युग
c) संगम काल
d) शिक्षा युग
उत्तर: b) स्वर्ण युग - किस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है?
a) रामायण
b) उपनिषद
c) मनुस्मृति
d) नाट्यशास्त्र
उत्तर: c) मनुस्मृति - किस काल में वर्ण और जाति प्रथा में कठोरता आई?
a) वैदिक काल
b) उत्तर वैदिक काल
c) मौर्य काल
d) गुप्त काल
उत्तर: b) उत्तर वैदिक काल
भाग 2
- सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन-सी थी?
a) ब्राह्मी
b) खरोष्ठी
c) चित्रलिपि
d) देवनागरी
उत्तर: c) चित्रलिपि - ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्त्वपूर्ण सभा कौन-सी थी?
a) सभा
b) समिति
c) विदथ
d) गण
उत्तर: a) सभा - महाजनपदों की संख्या कितनी थी?
a) 8
b) 10
c) 16
d) 18
उत्तर: c) 16 - महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था?
a) वैशाली
b) पाटलिपुत्र
c) कुंडग्राम
d) राजगृह
उत्तर: c) कुंडग्राम - बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था?
a) कुशीनगर
b) बोधगया
c) सारनाथ
d) लुंबिनी
उत्तर: c) सारनाथ - नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के समय प्रसिद्ध हुआ?
a) समुद्रगुप्त
b) कुमारगुप्त
c) हर्षवर्धन
d) स्कन्दगुप्त
उत्तर: b) कुमारगुप्त - किस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख मिलता है?
a) सामवेद
b) यजुर्वेद
c) ऋग्वेद
d) अथर्ववेद
उत्तर: c) ऋग्वेद - बौद्ध धर्म के अनुयायी किसे तिहारा रत्न (त्रिरत्न) मानते हैं?
a) बुद्ध, धर्म, संघ
b) बुद्ध, उपनिषद, संघ
c) बुद्ध, शंकराचार्य, संघ
d) धर्म, संघ, गुरु
उत्तर: a) बुद्ध, धर्म, संघ - वैदिक काल में विवाह की कौन सी प्रथा सामान्य थी?
a) बाल विवाह
b) स्वयंवर
c) विधवा विवाह
d) बहुपतित्व
उत्तर: b) स्वयंवर - किस ग्रंथ में शिक्षा की प्रणाली का वर्णन मिलता है?
a) मनुस्मृति
b) ब्राह्मण ग्रंथ
c) उपनिषद
d) स्मृति ग्रंथ
उत्तर: c) उपनिषद - बौद्ध धर्म के कौन-से संप्रदायों में विभाजन हुआ?
a) हीनयान और महायान
b) शैव और वैष्णव
c) स्थविरवाद और महायान
d) तांत्रिक और योगी
उत्तर: a) हीनयान और महायान - प्राचीन भारत में शिक्षक को क्या कहा जाता था?
a) आचार्य
b) पंडित
c) पुरोहित
d) गुरुजी
उत्तर: a) आचार्य - महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है?
a) बौद्ध ग्रंथ
b) वेद
c) उपनिषद
d) मनुस्मृति
उत्तर: a) बौद्ध ग्रंथ - ऋग्वैदिक काल में किस देवता को सबसे अधिक महत्त्व प्राप्त था?
a) अग्नि
b) इन्द्र
c) वरुण
d) सूर्य
उत्तर: b) इन्द्र - स्त्रियों को वैदिक काल में कौन सा अधिकार प्राप्त था?
a) संपत्ति का अधिकार
b) यज्ञ में भाग लेने का अधिकार
c) युद्ध में भाग लेने का अधिकार
d) शिक्षा में भाग लेने का अधिकार
उत्तर: d) शिक्षा में भाग लेने का अधिकार - किस स्थल से सिंधु सभ्यता की खुदाई नहीं हुई है?
a) मोहनजोदड़ो
b) हड़प्पा
c) लोथल
d) तक्षशिला
उत्तर: d) तक्षशिला - गार्गी कौन थीं?
a) एक ऋषि
b) एक विदुषी महिला
c) एक रानी
d) एक दासी
उत्तर: b) एक विदुषी महिला - बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को:
a) नकारा
b) स्वीकारा
c) संदेह किया
d) कुछ नहीं कहा
उत्तर: a) नकारा - वैदिक काल में ‘गृह्य सूत्र’ किससे संबंधित हैं?
a) धर्म
b) राजनीति
c) घरेलू कर्मकांड
d) युद्ध कला
उत्तर: c) घरेलू कर्मकांड - ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः क्या बताते हैं?
a) यज्ञों के विधि-विधान
b) दर्शनशास्त्र
c) चिकित्सा
d) राजनीति
उत्तर: a) यज्ञों के विधि-विधान
भारतीय संविधान के बारे में पढ़े – भारतीय संविधान का परिचय
- NCERT Class 6 History Chapter: What, Where, How and When?
- Ministry of Culture, Government of India
- CulturalIndia.net – Ancient Indian History
- Britannica – History of Ancient India
- World History Encyclopedia – Ancient India
- NCERT Official Website
- UNESCO – India and the Silk Road
- Archaeological Survey of India (ASI)