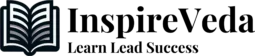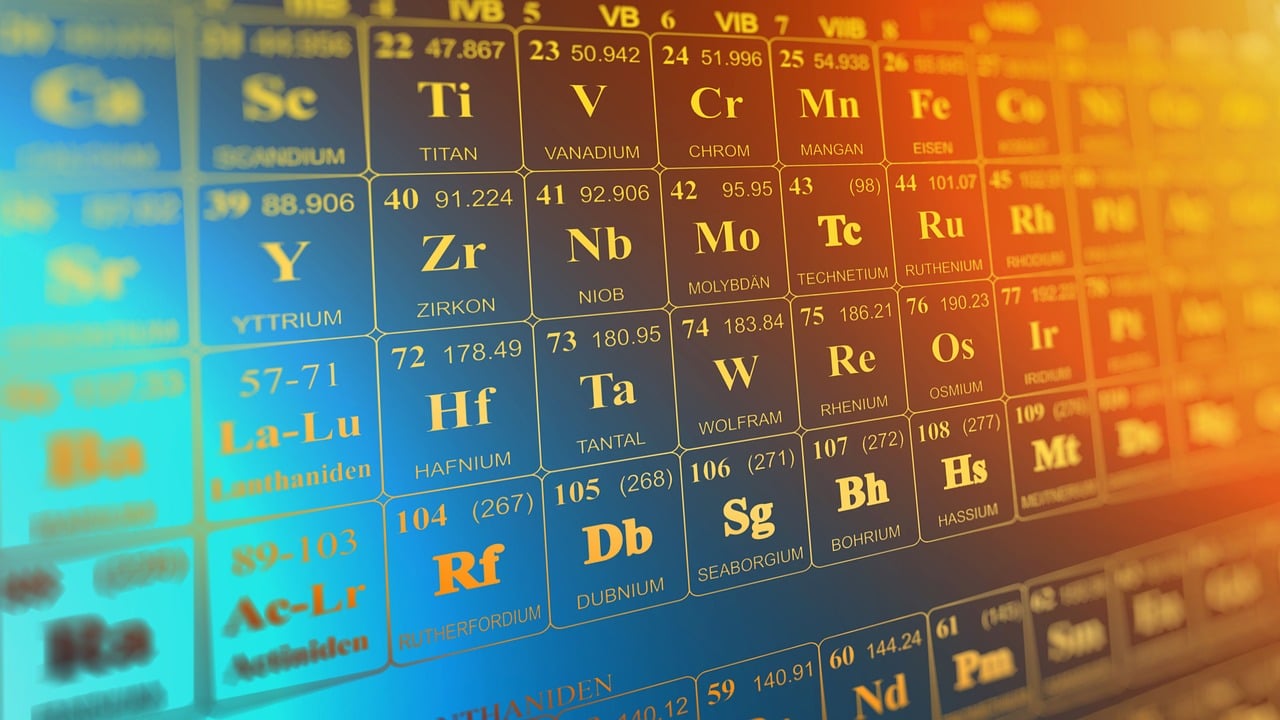धातु एवं अधातु – Class 10 Science Chapter 3
विज्ञान की दुनिया में धातु (Metals) और अधातु (Non-Metals) का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। हमारी दैनिक जीवन की बहुत-सी आवश्यक वस्तुएँ जैसे बर्तन, तार, गैस, ऑक्सीजन सिलिंडर, दवाइयाँ आदि इन्हीं तत्वों से बनी होती हैं। धातु और अधातु की भौतिक व रासायनिक विशेषताओं को समझना हमें यह जानने में मदद करता है कि कौन-से तत्व किस कार्य के लिए उपयुक्त हैं।
इस अध्याय में आप जानेंगे कि धातुएँ आमतौर पर चमकदार, तन्य और कुचालक क्यों होती हैं, जबकि अधातुएँ भंगुर और विद्युत की कुचालक क्यों होती हैं। साथ ही यह भी समझेंगे कि इनका रासायनिक व्यवहार, जैसे अम्ल और जल के साथ अभिक्रिया, एक-दूसरे से कैसे भिन्न होता है।
अंत में, आप यह भी जानेंगे कि धातुओं से संबंधित जंग लगना, उनके संरक्षण के उपाय और मिश्रधातुओं का निर्माण कैसे किया जाता है।
धातुओं के भौतिक गुणधर्म
धातुएँ (Metals) सामान्यतः ठोस, चमकदार, कठोर और अच्छी ताप तथा विद्युत चालक होती हैं। इनके गुणधर्म इन्हें दैनिक जीवन में उपयोगी बनाते हैं। नीचे दिए गए गुणधर्मों से हम धातुओं को आसानी से पहचान सकते हैं।
| भौतिक गुण | विवरण | उदाहरण |
|---|---|---|
| चमक (Lustre) | धातुओं की सतह चमकदार होती है। | सोना, चाँदी, तांबा |
| कठोरता (Hardness) | धातुएँ कठोर होती हैं, परन्तु कुछ नरम भी होती हैं। | सोडियम नरम, लोहा कठोर |
| तन्यता (Malleability) | धातुओं को पीटकर चादर में बदला जा सकता है। | एलुमिनियम, तांबा |
| नमनशीलता (Ductility) | धातुओं को तार में बदला जा सकता है। | सोना, चाँदी |
| ताप चालकता (Thermal Conductivity) | धातुएँ उष्मा को सुगमता से प्रवाहित करती हैं। | तांबा, एलुमिनियम |
| विद्युत चालकता (Electrical Conductivity) | धातुएँ विद्युत की सुचालक होती हैं। | तांबा, चाँदी |
| ध्वनि की गूंज (Sonorous) | धातुएँ चोट लगने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। | लोहे की घंटी, काँसा |
अधातुओं के भौतिक गुणधर्म
अधातुएँ (Non-Metals) सामान्यतः वे तत्व होते हैं जो धातुओं के विपरीत गुण दर्शाते हैं। ये मुख्यतः गैस या ठोस रूप में पाई जाती हैं (केवल ब्रोमिन तरल)। अधातुओं का उपयोग जीवन के अनेक क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे- ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आदि। इनके भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं:
| भौतिक गुण | विवरण | उदाहरण |
|---|---|---|
| स्थिति | अधातुएँ सामान्यतः गैस, कुछ ठोस, एक तरल होती हैं। | ऑक्सीजन (गैस), सल्फर (ठोस), ब्रोमिन (तरल) |
| चमक | अधातुएँ चमकहीन होती हैं। | कार्बन (कोयला), फॉस्फोरस |
| भंगुरता | अधातु ठोस अवस्था में भंगुर (brittle) होते हैं। | सल्फर, फॉस्फोरस |
| तन्यता व नमनशीलता | इनमें तन्यता व नमनशीलता नहीं होती। | नहीं पाया जाता |
| ताप व विद्युत चालकता | अधातुएँ कुचालक होती हैं (ग्रेफाइट अपवाद)। | सल्फर, क्लोरीन (कुचालक), ग्रेफाइट (सुचालक) |
| ध्वनि उत्पादन | अधातुएँ ध्वनि नहीं उत्पन्न करतीं। | कोई नहीं |
धातुओं के रासायनिक गुणधर्म
धातु केवल चमक, तन्यता और चालकता के लिए ही नहीं पहचाने जाते, बल्कि वे विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में भी भाग लेते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण उनके अभिक्रियाशील स्वभाव, अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया और यौगिक बनाने की क्षमता को दर्शाते हैं।
| रासायनिक गुणधर्म | विवरण | उदाहरण |
|---|---|---|
| ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया | धातु वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। | 4Na + O₂ → 2Na₂O |
| जल के साथ अभिक्रिया | कुछ धातुएँ जल से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हुए क्षार बनाती हैं। | 2K + 2H₂O → 2KOH + H₂ ↑ |
| अम्ल के साथ अभिक्रिया | धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाते हैं। | Zn + 2HCl → ZnCl₂ + H₂ ↑ |
| लवणों के साथ विस्थापन | सक्रिय धातुएँ कम सक्रिय धातुओं को उनके लवणों से विस्थापित कर देती हैं। | Fe + CuSO₄ → FeSO₄ + Cu |
Anodisation (ऐनोडीकरण)
परिभाषा:
Anodisation एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु (विशेषतः एल्युमिनियम) को इलेक्ट्रोलाइट में डुबोकर उसे ऐनोड बनाया जाता है, जिससे उसकी सतह पर सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनती है।
Anodisation की प्रक्रिया:
- एल्युमिनियम को ऐनोड (धनात्मक इलेक्ट्रोड) बनाया जाता है।
- इसे सल्फ्यूरिक अम्ल (H2SO4) जैसे इलेक्ट्रोलाइट में डुबोया जाता है।
- धारा प्रवाहित करने पर सतह पर ऑक्साइड परत (Al2O3) बनती है।
- यह परत धातु को जंग से बचाती है और उसे रंगने में मदद करती है।
Anodisation एक नियंत्रित ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जो धातु की सतह को सुरक्षित और आकर्षक बनाती है।
Anodisation के उद्देश्य:
| उद्देश्य | विवरण |
|---|---|
| सुरक्षा | जंग से बचाव के लिए सुरक्षात्मक परत बनती है। |
| सौंदर्य | रंगों के अवशोषण में मदद, सतह सुंदर बनती है। |
| मजबूती | सतह कठोर और टिकाऊ बनती है। |
| रासायनिक प्रतिरोध | रासायनिक प्रभावों से बचाव मिलता है। |
Anodisation के उपयोग:
- खिड़की फ्रेम और भवन सामग्री
- रसोई बर्तन और घरेलू उपकरण
- साइकिल और मोटर पार्ट्स
- एयरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया
सभी धातुएँ जल के साथ समान रूप से अभिक्रिया नहीं करतीं। कुछ धातुएँ जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती हैं, जबकि कुछ बहुत मंद गति से या बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करतीं। यह अभिक्रिया मुख्यतः हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन और धातु हाइड्रॉक्साइड के निर्माण के रूप में होती है।
सक्रिय धातुओं की जल से अभिक्रिया:
सोडियम (Na) और पोटैशियम (K) जैसी अत्यधिक सक्रिय धातुएँ ठंडे जल के साथ भी तीव्र प्रतिक्रिया करती हैं। ये धातुएँ जल के संपर्क में आते ही फूट पड़ती हैं और हाइड्रोजन गैस के साथ धातु हाइड्रॉक्साइड बनाती हैं। यह प्रक्रिया इतनी उष्माक्षमिक (exothermic) होती है कि हाइड्रोजन गैस जल उठती है।
उदाहरण:
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 ↑
मध्यम सक्रिय धातुएँ:
कैल्शियम (Ca) ठंडे जल के साथ प्रतिक्रिया करता है, लेकिन तीव्रता थोड़ी कम होती है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं और एक क्षारीय विलयन बनता है।
उदाहरण:
Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 ↑
कम सक्रिय धातुएँ:
एल्युमिनियम (Al), जिंक (Zn) और लोहा (Fe) जैसी धातुएँ सामान्य जल के साथ बहुत धीरे-धीरे प्रतिक्रिया करती हैं। लेकिन अगर जल गर्म हो या भाप हो, तो यह अभिक्रिया थोड़ी सक्रिय हो सकती है।
उदाहरण:
3Fe + 4H2O (g) → Fe3O4 + 4H2 ↑
अक्रिय धातुएँ:
सोना (Au), चांदी (Ag), ताँबा (Cu) जैसी धातुएँ जल या भाप के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करतीं। इन्हें अक्रिय धातुएँ (noble metals) कहा जाता है।
सोडियम और पोटैशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि ये नमी या जल के संपर्क में न आएँ, क्योंकि इनकी अभिक्रिया अत्यंत विस्फोटक होती है।
धातुओं का वायु में दहन
जब धातुओं को वायु (विशेषकर ऑक्सीजन) में गर्म किया जाता है, तो अधिकांश धातुएँ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। यह अभिक्रिया प्रायः उष्माक्षमिक (exothermic) होती है, जिसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं।
सक्रिय धातुएँ:
सोडियम (Na), पोटैशियम (K), कैल्शियम (Ca) आदि धातुएँ वायु में अत्यंत तीव्रता से जलती हैं। इनका दहन बहुत तेज़ होता है और ये श्वेत धुएँ के साथ धातु ऑक्साइड बनाती हैं।
उदाहरण:
4Na + O2 → 2Na2O
मध्यम क्रियाशील धातुएँ:
मैग्नीशियम (Mg), एल्यूमिनियम (Al), जिंक (Zn) जैसी धातुएँ हवा में आसानी से नहीं जलतीं, परंतु जब अत्यधिक गर्म की जाती हैं, तो ये जलती हैं और चमकीली रोशनी के साथ ऑक्साइड बनाती हैं।
उदाहरण:
2Mg + O2 → 2MgO
कम क्रियाशील धातुएँ:
लोहा (Fe), ताँबा (Cu) आदि वायु में सीधे नहीं जलते, लेकिन लंबे समय तक संपर्क में रहने पर ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके ऑक्साइड की परत बना लेते हैं।
उदाहरण:
4Fe + 3O2 → 2Fe2O3
अक्रिय धातुएँ:
सोना (Au) और चाँदी (Ag) जैसी धातुएँ वायु या ऑक्सीजन के साथ दहन नहीं करतीं। इन्हें अक्रिय धातुएँ कहा जाता है।
मैग्नीशियम को जलाने पर अत्यधिक चमकदार प्रकाश निकलता है, जिससे आँखों को नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रयोगशाला में इसे जलाते समय आँखों को सुरक्षित रखा जाता है।
धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया
जब धातुओं को अम्लों के साथ अभिक्रिया करने दिया जाता है, तो वे अम्ल के हाइड्रोजन आयन (H+) से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यह अभिक्रिया धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है।
सामान्य अभिक्रिया:
धातु + अम्ल → लवण + हाइड्रोजन गैस
उदाहरण के लिए:
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑
क्रियाशील धातुएँ:
जैसे-जैसे धातु अधिक क्रियाशील होती है, वह अम्लों के साथ उतनी ही तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम (Na), पोटैशियम (K), कैल्शियम (Ca) जैसी धातुएँ अत्यधिक तेजी से अम्लों के साथ क्रिया करती हैं और प्रयोगशाला में इनका उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाता है।
कम क्रियाशील धातुएँ:
ताँबा (Cu), चाँदी (Ag), सोना (Au) जैसी धातुएँ सामान्य अम्लों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करतीं क्योंकि ये कम क्रियाशील होती हैं। इन्हें प्रतिक्रिया कराने के लिए विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है।
अनुप्रयोग:
- अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन गैस का परीक्षण जलती तीली से किया जाता है, जिससे ‘पॉप’ ध्वनि आती है।
- इस प्रक्रिया का उपयोग धातु की क्रियाशीलता श्रृंखला निर्धारित करने में किया जाता है।
- धातु-अम्ल अभिक्रियाएँ स्कूल प्रयोगशालाओं में आमतौर पर की जाती हैं।
ताँबा (Cu) जैसे धातु, HCl और H2SO4 जैसे कमजोर अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि वे हाइड्रोजन आयनों को विस्थापित करने में अक्षम होती हैं।
अन्य धातु लवणों के साथ धातुओं की अभिक्रिया
जब कोई धातु किसी अन्य धातु के लवण विलयन के साथ अभिक्रिया करती है, तो उसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। यह अभिक्रिया तभी संभव है जब पहली धातु, दूसरी धातु से अधिक क्रियाशील हो।
मुख्य सिद्धांत:
अधिक क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती है। इसे एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है।
उदाहरण:
जब लोहे (Fe) की छड़ को ताँबे (CuSO4) के विलयन में डाला जाता है:
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu ↓
यहाँ Fe, Cu से अधिक क्रियाशील है और Cu को उसके लवण से विस्थापित कर देता है।
कैसे पहचानें कि अभिक्रिया हुई?
- विलयन का रंग बदल जाता है (उदाहरण: नीले रंग का विलयन हरा हो जाता है)।
- तल में नई धातु (जैसे ताँबा) के लाल-भूरे रंग की परत जम जाती है।
सोना (Au) और चाँदी (Ag) जैसी कम क्रियाशील धातुएँ, किसी भी लवण विलयन से अन्य धातुओं को विस्थापित नहीं कर सकतीं। परंतु पोटैशियम (K), सोडियम (Na), कैल्शियम (Ca) जैसी धातुएँ लगभग सभी धातुओं को उनके लवण से विस्थापित कर देती हैं।
उपयोग:
इस अभिक्रिया से हम क्रियाशीलता श्रेणी (Reactivity Series) को समझ सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि कौन-सी धातु अधिक क्रियाशील है।
सक्रियता श्रेणी (Reactivity Series) क्या है?
धातुओं की एक सूची जिसमें उन्हें उनकी रासायनिक क्रियाशीलता के अनुसार क्रमबद्ध किया गया हो, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यह श्रेणी यह निर्धारित करने में सहायक होती है कि कौन-सी धातु कितनी जल्दी और आसानी से अभिक्रियाएँ करती है, विशेष रूप से अम्लों, जल तथा अन्य धातु लवणों के साथ।
सक्रियता श्रेणी की परिभाषा:
यह धातुओं की वह क्रमबद्ध सूची है जो उनकी अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करने, जल से हाइड्रोजन विस्थापित करने एवं अन्य धातुओं को उनके लवणों से विस्थापित करने की क्षमता के आधार पर बनती है।
धातुओं की सक्रियता श्रेणी तालिका:
| क्रम | धातु का नाम | प्रतिक्रिया प्रवृत्ति |
|---|---|---|
| 1 | पोटैशियम (K) | अत्यंत क्रियाशील |
| 2 | सोडियम (Na) | अत्यंत क्रियाशील |
| 3 | कैल्शियम (Ca) | जल के साथ तीव्र प्रतिक्रिया |
| 4 | मैग्नीशियम (Mg) | उच्च प्रतिक्रिया |
| 5 | एलुमिनियम (Al) | तेज़ प्रतिक्रिया, ऑक्साइड परत बनती है |
| 6 | जिंक (Zn) | मध्यम क्रियाशील |
| 7 | लोहा (Fe) | धीमी प्रतिक्रिया |
| 8 | सीसा (Pb) | कम क्रियाशील |
| 9 | हाइड्रोजन (H) | संदर्भ बिंदु |
| 10 | कॉपर (Cu) | बहुत कम क्रियाशील |
| 11 | मर्करी (Hg) | बहुत ही कम प्रतिक्रिया |
| 12 | सिल्वर (Ag) | लगभग अक्रियाशील |
| 13 | गोल्ड (Au) | निष्क्रिय |
| 14 | प्लैटिनम (Pt) | निष्क्रिय |
अधिक क्रियाशील धातुएँ कम क्रियाशील धातुओं को उनके लवणों से विस्थापित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, जिंक (Zn) ताँबे के लवण को विस्थापित कर सकता है लेकिन कॉपर (Cu) ऐसा नहीं कर सकता।
सक्रियता श्रेणी का प्रयोग:
- धातुओं की तुलना करना (कौन अधिक क्रियाशील है)।
- अम्ल और जल से प्रतिक्रिया की संभावना ज्ञात करना।
- धातु लवणों की विस्थापन अभिक्रिया का पूर्वानुमान लगाना।
- खनिजों से धातु निष्कर्षण में मदद।
सक्रियता श्रेणी को याद रखने का तरीका:
एक सरल वाक्य जैसे — “Please Stop Calling Me A Zebra; I Like Her Call Smart Girl Pretty”
(Potassium, Sodium, Calcium, Magnesium, Aluminium, Zinc, Iron, Lead, Hydrogen, Copper, Silver, Gold, Platinum)
धातुओं और अधातुओं के बीच अभिक्रिया (Reaction between Metals and Non-metals)
जब धातु और अधातु परस्पर अभिक्रिया करते हैं, तो वे इलेक्ट्रॉनों का आदान-प्रदान करते हैं और आयनी यौगिक (Ionic Compounds) बनाते हैं। इस प्रक्रिया में धातु इलेक्ट्रॉन दान करती है और अधातु इलेक्ट्रॉन स्वीकार करती है।
धातु हमेशा धनायन (Cation) बनाती है जबकि अधातु ऋणायन (Anion) बनाती है।
इस अभिक्रिया की प्रक्रिया:
- धातु → इलेक्ट्रॉन दान करती है → धनायन (M+) बनता है
- अधातु → इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है → ऋणायन (X–) बनता है
- धनायन + ऋणायन → आयनिक यौगिक (MX)
उदाहरण:
सोडियम (Na) + क्लोरीन (Cl) → सोडियम क्लोराइड (NaCl)
- Na → Na+ + e–
- Cl + e– → Cl–
- Na+ + Cl– → NaCl (आयनी यौगिक)
अभिक्रिया के उत्पाद की विशेषताएँ:
- अधिक घुलनशीलता जल में
- उच्च गलनांक और क्वथनांक
- विद्युत चालकता युक्त (घोल या पिघले रूप में)
यह अभिक्रिया हमेशा एक आयनिक यौगिक का निर्माण करती है, जो धातु और अधातु के बीच की परस्पर क्रिया का परिणाम होता है।
अन्य उदाहरण:
- मैग्नीशियम + ऑक्सीजन → मैग्नीशियम ऑक्साइड (MgO)
- एलुमिनियम + नाइट्रोजन → एलुमिनियम नाइट्राइड (AlN)
- कैल्शियम + सल्फर → कैल्शियम सल्फाइड (CaS)
20 प्रमुख तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास (Electronic Configuration of First 20 Elements)
| परमाणु क्रमांक | तत्व | प्रतीक | इलेक्ट्रॉनिक विन्यास |
|---|---|---|---|
| 1 | हाइड्रोजन | H | 1 |
| 2 | हीलियम | He | 2 |
| 3 | लिथियम | Li | 2,1 |
| 4 | बेरिलियम | Be | 2,2 |
| 5 | बोरॉन | B | 2,3 |
| 6 | कार्बन | C | 2,4 |
| 7 | नाइट्रोजन | N | 2,5 |
| 8 | ऑक्सीजन | O | 2,6 |
| 9 | फ्लोरीन | F | 2,7 |
| 10 | निऑन | Ne | 2,8 |
| 11 | सोडियम | Na | 2,8,1 |
| 12 | मैग्नीशियम | Mg | 2,8,2 |
| 13 | एल्युमिनियम | Al | 2,8,3 |
| 14 | सिलिकॉन | Si | 2,8,4 |
| 15 | फॉस्फोरस | P | 2,8,5 |
| 16 | सल्फर | S | 2,8,6 |
| 17 | क्लोरीन | Cl | 2,8,7 |
| 18 | आर्गन | Ar | 2,8,8 |
| 19 | पोटैशियम | K | 2,8,8,1 |
| 20 | कैल्शियम | Ca | 2,8,8,2 |
आयनिक यौगिकों के गुणधर्म (Properties of Ionic Compounds)
आयनिक यौगिक वे रासायनिक यौगिक होते हैं जो धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा बनते हैं। इनमें धनायन (cation) और ऋणायन (anion) के बीच बलवान वैद्युत स्थैतिक आकर्षण होता है।
आयनिक यौगिकों के प्रमुख गुणधर्म:
- 1. उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक: आयनिक यौगिकों में आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, इसलिए इन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
- 2. ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन नहीं करते: ठोस अवस्था में आयन गतिशील नहीं होते, इसलिए विद्युत चालकता नहीं होती।
- 3. जलीय विलयन अथवा पिघली अवस्था में विद्युत चालक: जब आयनिक यौगिक पानी में घुलते हैं या पिघलते हैं, तो आयन स्वतंत्र हो जाते हैं और विद्युत धारा का संचालन करते हैं।
- 4. भंगुरता (Brittleness): आयनिक यौगिक कठोर होते हैं लेकिन आसानी से टूट सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आयन अपनी स्थिति बदलते हैं, एक जैसे आवेश वाले आयन एक-दूसरे के पास आ जाते हैं, जिससे विकर्षण होता है और पदार्थ टूट जाता है।
- 5. जल में विलेयता: अधिकांश आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ जैसे बैरियम सल्फेट (BaSO₄) और सिल्वर क्लोराइड (AgCl) जल में अघुलनशील होते हैं।
🧪 उदाहरण:
- NaCl (सोडियम क्लोराइड)
- MgO (मैग्नीशियम ऑक्साइड)
- CaCl₂ (कैल्शियम क्लोराइड)
कुछ आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक
| आयनिक यौगिक | रासायनिक सूत्र | गलनांक (°C) | क्वथनांक (°C) |
|---|---|---|---|
| सोडियम क्लोराइड | NaCl | 801 | 1465 |
| मैग्नीशियम ऑक्साइड | MgO | 2852 | 3600 |
| कैल्शियम क्लोराइड | CaCl₂ | 772 | 1935 |
| एल्यूमीनियम ऑक्साइड | Al₂O₃ | 2072 | 2977 |
| लिथियम फ्लोराइड | LiF | 848 | 1676 |
धातुओं का निष्कर्षण (Extraction of Metals)
पृथ्वी की परतों में धातुएँ विभिन्न यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, जिन्हें अयस्क (Ores) कहते हैं। धातुओं को उनके अयस्कों से अलग करके शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु निष्कर्षण कहते हैं। यह प्रक्रिया मुख्यतः धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है।
धातुओं की क्रियाशीलता के अनुसार निष्कर्षण की विधियाँ
| क्रियाशीलता | उदाहरण | निष्कर्षण विधि |
|---|---|---|
| अत्यधिक क्रियाशील | Na, K, Ca, Mg, Al | विद्युत अपघटन (Electrolysis) |
| मध्यम क्रियाशील | Zn, Fe, Pb, Cu | अयस्क का पहले रोस्टिंग/कैल्सिनेशन, फिर विस्थापन |
| कम क्रियाशील | Hg, Ag, Au | अयस्क को गरम करने पर सीधा धातु प्राप्त |
निष्कर्षण के चरण (Steps of Metal Extraction)
- अयस्क का सांद्रीकरण (Concentration): अपद्रव्यों को हटाकर अयस्क की शुद्धता बढ़ाना।
- अपचयन (Reduction): धातु के ऑक्साइड को धातु में बदलना (जैसे कोक द्वारा)।
- शुद्धिकरण (Purification): विद्युत अपघटन या अन्य विधियों से शुद्ध धातु प्राप्त करना।
मुख्य अयस्क और संबंधित धातु
| धातु | मुख्य अयस्क | रासायनिक सूत्र |
|---|---|---|
| एलुमिनियम | बॉक्साइट | Al₂O₃·xH₂O |
| लोहा | हैमेटाइट | Fe₂O₃ |
| जस्ता | जिंक ब्लेन्ड | ZnS |
धातुओं का निष्कर्षण (Extraction of Metals)
धातुओं को उनके अयस्कों (Ore) से निकालने की प्रक्रिया को धातु निष्कर्षण कहते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से धातु की अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है।
1. अयस्क का सांद्रण (Concentration of Ore)
- अयस्क में अपद्रव्य (gangue) होते हैं जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों से हटाया जाता है।
- उदाहरण: वायुवीक्षण, प्रवाही प्रकीर्णन, चुंबकीय पृथक्करण, फ्रोथ फ्लोटेशन।
2. धातु की अभिक्रियाशीलता के आधार पर निष्कर्षण विधियाँ
(A) उच्च अभिक्रियाशील धातुएँ
- उदाहरण: Na, K, Ca, Al
- गले हुए अयस्क का विद्युत अपघटन किया जाता है।
- शुद्ध धातु प्राप्त होती है।
(B) मध्यम अभिक्रियाशील धातुएँ
- उदाहरण: Zn, Fe, Pb, Cu
- कार्बोनेट अयस्क → निस्तापन
- सल्फाइड अयस्क → भंजन
- फिर अपचयन द्वारा धातु प्राप्त की जाती है।
(C) निम्न अभिक्रियाशील धातुएँ
- उदाहरण: Ag, Au, Pt
- अक्सर मुक्त रूप में पाई जाती हैं।
- भंजन या परिशोधन से प्राप्त होती हैं।
3. धातु का शोधन (Purification of Metal)
- प्राप्त धातु अशुद्ध होती है, उसे शुद्ध करने के लिए:
- विद्युत शोधन (Electrolytic refining), आसवन, वाष्पीय शोधन, अमलगम विधि आदि अपनाई जाती हैं।
निष्कर्ष तालिका
| धातु की श्रेणी | निष्कर्षण विधि |
|---|---|
| उच्च अभिक्रियाशील | विद्युत अपघटन द्वारा |
| मध्यम अभिक्रियाशील | भंजन/निस्तापन → अपचयन |
| निम्न अभिक्रियाशील | भौतिक विधियाँ या परिशोधन |
🔹 निस्तापन = कार्बोनेट अयस्क को बिना वायु के गर्म करना
🔹 भंजन = सल्फाइड अयस्क को वायु में गर्म करना
🔹 अपचयन = धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना
🔹 विद्युत अपघटन = उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के लिए आवश्यक
भर्जन एवं निस्तापन (Roasting and Calcination)
अयस्कों से अशुद्धियाँ हटाने के लिए उन्हें गर्म करने की दो प्रमुख विधियाँ होती हैं:
(1) भर्जन और (2) निस्तापन।
1. भर्जन (Roasting)
- सल्फाइड अयस्कों को अधिक ताप पर अधिक मात्रा में वायु की उपस्थिति में गर्म करना।
- इससे अयस्क का सल्फाइड ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है।
2ZnS + 3O2 → 2ZnO + 2SO2(जिंक ब्लेंड → जिंक ऑक्साइड + सल्फर डाइऑक्साइड)
2PbS + 3O2 → 2PbO + 2SO2(गैलेना → सीसा ऑक्साइड + सल्फर डाइऑक्साइड)
2. निस्तापन (Calcination)
- कार्बोनेट या हाइड्रॉक्साइड अयस्कों को अधिक ताप पर वायु की अनुपस्थिति या सीमित वायु में गर्म करना।
- इससे अयस्क का कार्बोनेट ऑक्साइड में बदलता है और CO2 गैस निकलती है।
CaCO3 → CaO + CO2(कैल्सियम कार्बोनेट → क्विक लाइम + कार्बन डाइऑक्साइड)
ZnCO3 → ZnO + CO2(सिंक कार्बोनेट → जिंक ऑक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड)
अंतर सारणी (Roasting vs Calcination)
| मापदंड | भर्जन | निस्तापन |
|---|---|---|
| वायु की उपस्थिति | वायु में गर्म करना | वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना |
| अयस्क का प्रकार | सल्फाइड अयस्क | कार्बोनेट / हाइड्रॉक्साइड अयस्क |
| उत्पन्न गैस | SO2 | CO2 |
☑ भर्जन = सल्फाइड अयस्क + वायु
☑ निस्तापन = कार्बोनेट अयस्क + वायु रहित ताप
सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण
सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएँ अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं। इन्हें उनके अयस्क से निकालने के लिए सामान्य रासायनिक विधियाँ जैसे भर्जन या निस्तापन पर्याप्त नहीं होतीं।
➤ निष्कर्षण विधि: विद्युत अपघटन (Electrolytic Reduction)
इन धातुओं को उनके पिघले हुए (Molten) अयस्कों का विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है।
NaCl (molten) → Na(cathode) + Cl2(gas at anode)सोडियम क्लोराइड को पिघला कर विद्युत अपघटन करने पर:
➤ कैथोड पर – धातु (Na)
➤ एनोड पर – गैस (Cl2) निकलती है।
बोक्साइट (Al2O3) को क्रायोलाइट के साथ मिलाकर पिघलाया जाता है और विद्युत अपघटन किया जाता है:
Al2O3 (molten) → Al(cathode) + O2(anode)कारण क्यों अन्य विधियाँ उपयोगी नहीं:
- ये धातुएँ ऑक्सीजन और अन्य तत्वों से बहुत मज़बूती से जुड़ी होती हैं।
- रासायनिक विधियों द्वारा इन्हें निकालना कठिन होता है।
- इसलिए इनका निष्कर्षण केवल विद्युत द्वारा संभव है।
सक्रियता श्रेणी में ऊपर की धातुएँ जैसे Na, K, Ca, Mg, Al आदि का निष्कर्षण हमेशा विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय होती हैं।
सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण
सक्रियता श्रेणी की मध्य स्थित धातुएँ – जैसे जिंक (Zn), आयरन (Fe), लेड (Pb), कॉपर (Cu) – इतनी सक्रिय नहीं होतीं कि उनके निष्कर्षण के लिए विद्युत अपघटन जरूरी हो। इनका निष्कर्षण रासायनिक विधियों द्वारा किया जाता है।
➤ मुख्य निष्कर्षण विधियाँ:
- भर्जन (Roasting): जब अयस्क सल्फाइड रूप में होता है, तो उसे वायु में गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदला जाता है।
- निस्तापन (Calcination): जब अयस्क हाइड्रॉक्साइड या कार्बोनेट रूप में होता है, तो उसे बिना वायु के गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है।
- इसके बाद धातु ऑक्साइड को किसी अपचायक जैसे कार्बन (कोक) की सहायता से धातु में बदला जाता है।
उदाहरण 1: जिंक का निष्कर्षण
भर्जन:
2ZnS + 3O2 → 2ZnO + 2SO2निस्तापन:
ZnO + C → Zn + COउदाहरण 2: आयरन का निष्कर्षण
निस्तापन:
Fe2O3 + 3C → 2Fe + 3COयह क्रिया ब्लास्ट फर्नेस में होती है।
निष्कर्ष:
- मध्य स्थित धातुएँ विद्युत अपघटन से नहीं, बल्कि रासायनिक क्रियाओं द्वारा निकाली जाती हैं।
- भर्जन और निस्तापन द्वारा अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है।
- फिर अपचायक (जैसे कोक) की मदद से शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है।
सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित धातुओं का निष्कर्षण
सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित धातुएँ (जैसे: सोना, चाँदी, प्लेटिनम) अत्यंत निम्न अभिक्रियाशील होती हैं। ये प्राकृतिक अवस्था में अक्सर मुक्त रूप (Free State) में पाई जाती हैं। इन्हें निष्कर्षित करने के लिए अधिक रासायनिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती।
➤ निष्कर्षण की विधियाँ:
- प्राकृतिक अवस्था में मुक्त रूप: ये धातुएँ अक्सर पृथ्वी में स्वयं शुद्ध रूप में पाई जाती हैं, जैसे – सोने की डली।
- यांत्रिक पृथक्करण: रेत, मिट्टी या चट्टानों से इन्हें **छलनी**, **धोने**, या **झारने** की विधियों से अलग किया जाता है।
- सायनाइड विधि (Cyanide Process): विशेषतः सोने और चाँदी के लिए यह रासायनिक विधि उपयोगी होती है।
सोने का निष्कर्षण: सायनाइड विधि
4Au + 8NaCN + 2H2O + O2 → 4Na[Au(CN)2] + 4NaOHफिर जिंक मिलाकर शुद्ध सोना निकाला जाता है:2Na[Au(CN)2] + Zn → Na2[Zn(CN)4] + 2Auचाँदी का निष्कर्षण:
4Ag + 8NaCN + O2 + 2H2O → 4Na[Ag(CN)2] + 4NaOH निष्कर्ष:
- ये धातुएँ इतनी कम सक्रिय होती हैं कि प्रकृति में स्वतः मुक्त रूप में मिल जाती हैं।
- सायनाइड विधि इनका प्रमुख रासायनिक निष्कर्षण तरीका है।
- इनके निष्कर्षण में उच्च ताप या अधिक रासायनिक प्रतिक्रियाएँ नहीं चाहिए होतीं।
धातुओं का परिष्करण (Refining of Metals)
जब धातुओं को अयस्क से निष्कर्षित किया जाता है तो वे पूरी तरह शुद्ध नहीं होतीं। इनमें अन्य धातुएँ या अशुद्धियाँ मिली होती हैं। इन अशुद्धियों को हटाकर धातु को शुद्ध करने की प्रक्रिया को परिष्करण या Refining कहा जाता है।
परिष्करण की प्रमुख विधियाँ:
| विधि | मुख्य उपयोग | विवरण |
|---|---|---|
| 1. विद्युत अपघटन विधि (Electrolytic Refining) | ताँबा, जस्ता, सोना, चाँदी आदि | इस विधि में अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु को कैथोड बनाया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाती है। |
| 2. आसवन विधि (Distillation) | पारा (Mercury), जिंक | इस विधि में धातु को वाष्प बनाकर फिर उसे संघनित किया जाता है ताकि अशुद्धियाँ पीछे छूट जाएँ। |
| 3. वाष्पिकरण विधि (Vapour Phase Refining) | Titanium, Nickel | धातु को एक रासायनिक यौगिक में परिवर्तित किया जाता है जो गैस बन सके और फिर उसे पुनः विघटित कर शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। |
| 4. क्षेत्र परिष्करण (Zone Refining) | Silicon, Germanium | यह विधि अर्धचालकों (semiconductors) के परिष्करण में उपयोग की जाती है। इसमें एक गर्म क्षेत्र को धीरे-धीरे क्रिस्टल के ऊपर ले जाया जाता है जिससे अशुद्धियाँ एक दिशा में एकत्र हो जाती हैं। |
विद्युत अपघटन विधि का उदाहरण: ताँबे (Cu) का परिष्करण
- एनोड: अशुद्ध ताँबे की प्लेट
- कैथोड: शुद्ध ताँबे की पतली प्लेट
- इलेक्ट्रोलाइट: ताँबे का सल्फेट (CuSO₄) विलयन
- परिणाम: शुद्ध ताँबा कैथोड पर जमता है और अशुद्धियाँ तलछट के रूप में नीचे गिरती हैं जिसे एनोड कीचड़ (anode mud) कहते हैं।
निष्कर्ष:
- धातुओं के परिष्करण से उनकी उपयोगिता और शुद्धता बढ़ती है।
- अलग-अलग धातुओं के लिए उपयुक्त परिष्करण विधि चुनी जाती है।
- शुद्ध धातुएँ विद्युत, दवा, उद्योग और आभूषण जैसे क्षेत्रों में उपयोग की जाती हैं।
संक्षारण एवं इससे सुरक्षा
जब धातु वायुमंडलीय आर्द्रता, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के संपर्क में आती है, तो वह धीरे-धीरे नष्ट हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण (Corrosion) कहते हैं।
उदाहरण:
- लोहे पर जंग लगना (Fe → Fe₂O₃.xH₂O)
- ताँबे पर हरे रंग की परत बनना
- चाँदी का काला पड़ जाना
संक्षारण के दुष्परिणाम:
- धातु की मजबूती कम हो जाती है।
- मशीनरी और ढाँचे कमजोर हो जाते हैं।
- आर्थिक नुकसान होता है।
संक्षारण से सुरक्षा के उपाय:
- 1. गैल्वेनाइजेशन: लोहे की वस्तुओं को जिंक की परत से ढंकना।
- 2. तैलन/चिकनाई: मशीन के भागों पर तेल या ग्रीस लगाना।
- 3. चित्रण (Painting): धातु की सतह पर पेंट लगाकर वायु और नमी से बचाव।
- 4. एनोडिक सुरक्षा: सक्रिय धातु का उपयोग कर अधिक प्रतिक्रियाशील धातु को पहले संक्षारित करना।
- 5. मिश्रधातुएँ बनाना: जैसे स्टेनलेस स्टील जिसमें क्रोमियम होता है जो जंग से बचाव करता है।
- 6. विद्युत रासायनिक संरक्षण: धातु को कैथोड बनाकर बैटरी के माध्यम से सुरक्षा।
जंग लगने की रासायनिक अभिक्रिया:
यह लाल-भूरी परत होती है जिसे हम जंग (Rust) कहते हैं।
निष्कर्ष:
- संक्षारण एक हानिकारक प्रक्रिया है जो धातुओं की गुणवत्ता को खराब करती है।
- रासायनिक उपायों और यांत्रिक सुरक्षा विधियों से इसे रोका जा सकता है।
पाठ का सारांश:-
धातु क्या हैं?
वे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, हथौड़ी से पीटने पर चादर में बदले जा सकते हैं और तारों में खींचे जा सकते हैं, उन्हें धातु कहा जाता है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसी कारण से ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं।
धातु एवं अधातु
धातुओं के भौतिक गुण:
- चमकीले (लस्टरस): चमक का गुण
- तन्य (Ductile): खींचने पर लंबाई में बढ़ जाने का गुण
- आघातवर्ध्य (Malleable)
- ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक: मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण
- ठोस अवस्था में होते हैं (पारा को छोड़कर): पर द्रव अवस्था में होता है।
धातुओं के रासायनिक गुण:
- धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाते हैं।
उदाहरण: 4Na + O2 → 2Na2O - धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं।
उदाहरण: 2K + 2H2O → 2KOH + H2 - धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं।
उदाहरण: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 - धातुएं नमक के विलयन से कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर सकते हैं।
अधातु क्या हैं?
वे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के खराब चालक होते हैं,क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं ।भंगुर होते हैं और धातुओं के विपरीत गुण रखते हैं, उन्हें अधातु कहा जाता है। अधातुओं में ब्रोमिन द्रव रूप में होती है।
अधातुओं के भौतिक गुण:
- अधातुओं में चमक का गुण नहीं होता हैं (आयोडीन को छोड़कर)
- भंगुर (Brittle) होती हैं
- ऊष्मा और विद्युत के कुचालक (Graphite अपवाद है)
- गैस, तरल या ठोस तीनों अवस्था में मिलते हैं।
अधातुओं के रासायनिक गुण:
- धातुओं के साथ अभिक्रियाएं करके लवण बनाते हैं।
- ऑक्सीजन के साथ अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं।
उदाहरण: C + O2 → CO2 - धातुओं से इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बनाते हैं।
धातुओं एवं अधातुओं के बीच मुख्य अंतर:
| विशेषता | धातु | अधातु |
|---|---|---|
| दिखावट | चमकीले | मैट (धुंधले) |
| आघातवर्ध्यता | हाँ | नहीं |
| तन्यता | हाँ | नहीं |
| ऊष्मा चालकता | अच्छे चालक | कुचालक |
| ध्वनि चालकता | हाँ (सोनोरस) | नहीं |
आवश्यक अभिक्रियाएं:
- धातु + ऑक्सीजन → धात्विक ऑक्साइड
- धातु + पानी → क्षार + हाइड्रोजन गैस
- धातु + अम्ल → लवण + हाइड्रोजन गैस
धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी (Reactivity Series):
यह एक सूची है जो धातुओं को उनकी रासायनिक क्रियाशीलता के अनुसार क्रम में दर्शाती है।
- सबसे ऊपर: पोटैशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम
- मध्य: जिंक, आयरन, टिन
- निचले स्तर: कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड
धातु एवं अधातु
मिश्रातु (Alloys):
दो या दो से अधिक धातुओं (या धातु + अधातु) का मिश्रण जिसे विशेष गुणों के लिए तैयार किया जाता है।
- स्टेनलेस स्टील = लोहा + क्रोमियम + निकेल
- ब्रास = तांबा + जिंक
- ब्रॉन्ज = तांबा + टिन
धातुओं का संक्षारण:
जब धातुएं वायु, जल या अन्य रसायनों के संपर्क में आकर अभिक्रियाएं करती हैं, तो वे खराब होने लगती हैं, जिसे संक्षारण कहते हैं।
उदाहरण: लोहे में जंग लगना
धातु एवं अधातु से पाठ्य निहित प्रश्नों के उत्तर:-
प्रश्न 1. ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो
(i) कमरे के ताप पर द्रव होती है:
➡ पारा (Mercury) – यह एकमात्र धातु है जो सामान्य तापमान पर भी द्रव रूप में पाई जाती है। थर्मामीटर में आपने देखा होगा!
(ii) चाकू से आसानी से काटा जा सकता है:
➡ सोडियम (Sodium) – यह इतनी मुलायम धातु होती है कि चाकू से भी आराम से काटी जा सकती है। लेकिन ध्यान रहे, इसे हवा से बचाकर रखना पड़ता है क्योंकि ये बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करती है।
(iii) ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है:
➡ चाँदी (Silver) – यह ऊष्मा और विद्युत दोनों की सबसे बेहतरीन चालक होती है, लेकिन महंगी होने के कारण रोज़मर्रा के उपकरणों में कम उपयोग होती है।
(iv) ऊष्मा की कुचालक होती है:
➡ सीसा (Lead) – यह धातु गर्मी को आगे नहीं बढ़ने देती, यानी यह ऊष्मा की कुचालक होती है।
प्रश्न 2. आघातवर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए:
▶ आघातवर्ध्य (Malleable) का अर्थ:
जब कोई धातु हथौड़े या मशीन से पीटने पर टूटे नहीं बल्कि फैलकर पतली चादर में बदल जाए, तो उसे आघातवर्ध्य कहते हैं।
जैसे: तांबा (Copper), सोना (Gold)
▶ तन्य (Ductile) का अर्थ:
जब किसी धातु को खींचकर बिना तोड़े पतला तार बनाया जा सके, तो वह तन्य कहलाती है।
जैसे: एलुमिनियम (Aluminium), तांबा (Copper)
धातु एवं अधातु
प्रश्न 3:
(i) सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन-बिंदु संरचना लिखिए।
उत्तर:
Na (सोडियम): Na•
O (ऑक्सीजन): ••O•• (कुल 6 बिंदु)
Mg (मैग्नीशियम): •Mg•
(ii) इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na₂O एवं MgO का निर्माण दर्शाइए।
-
- 2Na → 2Na⁺ + 2e⁻
- O + 2e⁻ → O²⁻
- ⇒ Na₂O में Na⁺ और O²⁻ आयन
- Mg → Mg²⁺ + 2e⁻
- O + 2e⁻ → O²⁻
- ⇒ MgO में Mg²⁺ और O²⁻ आयन
(iii) इन यौगिकों में कौन-कौन से आयन उपस्थित हैं?
- Na₂O में – Na⁺ और O²⁻
- MgO में – Mg²⁺ और O²⁻
आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है?
उत्तर: क्योंकि इनमें धनायन और ऋणायन के बीच मजबूत विद्युत आकर्षण बल होता है जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए होती है।
प्रश्न 4:
(i) खनिज, अपस्क एवं गैंग की परिभाषा:
- खनिज: पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिनसे धातु प्राप्त की जा सकती है।
- अपस्क (अयस्क): वे खनिज जिनसे लाभकारी रूप से धातु निकाली जा सकती है।
- गैंग: अयस्कों में पाए जाने वाले बेकार अवांछित पदार्थ जैसे – रेत, मिट्टी।
(ii) दो धातुओं के नाम जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं:
- सोना (Gold)
- चाँदी (Silver)
धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए कौन-सा प्रक्रम उपयोग में लिया जाता है?
उत्तर: अपचयन (Reduction) प्रक्रिया। जैसे कार्बन या एलुमिनियम की सहायता से।
प्रश्न 5:
जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के ऑक्साइड को विभिन्न धातुओं से गर्म करने पर विस्थापन किस स्थिति में होगा?
| प्रयोग | विस्थापन होगा? | कारण |
|---|---|---|
| जिंक ऑक्साइड + मैग्नीशियम | हां | Mg > Zn |
| जिंक ऑक्साइड + कॉपर | नहीं | Cu < Zn |
| मैग्नीशियम ऑक्साइड + जिंक | नहीं | Zn < Mg |
| मैग्नीशियम ऑक्साइड + कॉपर | नहीं | Cu < Mg |
| कॉपर ऑक्साइड + जिंक | हां | Zn > Cu |
| कॉपर ऑक्साइड + मैग्नीशियम | हां | Mg > Cu |
प्रश्न 5:
कौन-सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है?
उत्तर: सोना (Gold) और प्लैटिनम (Platinum) – ये अभिक्रियाशीलता में बहुत कम होती हैं, इसलिए ये संक्षारण (corrosion) से नहीं खराब होतीं।
प्रश्न 6:
मिश्रातु क्या होते हैं?
उत्तर: जब दो या अधिक धातुओं (या धातु + अधातु) को पिघलाकर मिलाया जाता है तो जो पदार्थ बनता है, उसे मिश्रातु (Alloy) कहते हैं। ये शुद्ध धातु की तुलना में अधिक उपयोगी होते हैं।
उदाहरण:
- पीतल (Brass) = तांबा + जिंक
- ब्रॉन्ज (Bronze) = तांबा + टिन
- स्टेनलेस स्टील = लोहा + क्रोमियम + निकेल
पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर:
1. निम्नलिखित में कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है—
उत्तर: (d) AgNO₃ विलयन एवं तांबा धातु
स्पष्टीकरण: चांदी (Ag) की तुलना में तांबा (Cu) अधिक क्रियाशील होता है। इसलिए तांबा, चांदी को उसके लवण से विस्थापित कर देता है। यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है।
2. लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है—
उत्तर: (d) ऊपर के सभी
स्पष्टीकरण: जंग से बचाने के लिए लोहे पर तेल लगाना, पेंट करना या जिंक की परत चढ़ाना सभी प्रभावी तरीके हैं।
3. कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है?
उत्तर: (a) कैल्सियम
स्पष्टीकरण: कैल्सियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कैल्सियम ऑक्साइड बनाता है जो उच्च गलनांक वाला होता है और जल में घुलनशील है।
4. खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर टिन के बजाय जिंक का लेप नहीं होता है, क्योंकि—
उत्तर: (c) टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है
स्पष्टीकरण: यदि जिंक का प्रयोग किया जाए तो वह खाद्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया कर सकता है, क्योंकि वह अधिक अभिक्रियाशील है। टिन अपेक्षाकृत कम सक्रिय होता है, इसलिए सुरक्षित होता है।
5. आपको एक छड़ियां, बेलन, ब्लेड, तार एवं द्विवध दिया गया है—
उत्तर:
(a) इन वस्तुओं को देखकर हम उनके गुण (जैसे चमक, कठोरता, चालकता आदि) की तुलना करके यह बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु धातु की बनी है और कौन सी अधातु की।
(b) धातु और अधातु के बीच भिन्नता जानने के लिए आप परीक्षण कर सकते हैं – जैसे तार में विद्युत चालकता, छड़ को पीटकर देखने पर वह चपटी होती है या टूटती है, आदि। ये प्रयोग उन्हें पहचानने में मदद करेंगे।
6. उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए।
उत्तर: वे धात्विक ऑक्साइड जो जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं।
उदाहरण:Al2O3 और ZnO
7. दो धातुओं के नाम बताइए, जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दें तथा दो धातुएँ जो ऐसा नहीं कर सकती हैं।
उत्तर:
जो विस्थापित करती हैं: जिंक, लोहा
जो नहीं करती हैं: तांबा, चाँदी
8. किसी धातु में विद्युत अपघटन प्रयोग करते समय एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे?
उत्तर:
– एनोड: अशुद्ध धातु होती है।
– कैथोड: शुद्ध धातु की छड़ होती है।
– विद्युत अपघट्य: उस धातु का लवणीय विलयन (जैसे कॉपर सल्फेट)।
9. प्रयोग में सल्फर चूर्ण को स्पैटुला से लेकर उसे गर्म किया गया। गैस की पहचान एवं रासायनिक अभिक्रिया लिखिए।
(a) गैस की क्रिया:
(i) सूखे लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं।
(ii) गीले लिटमस पर यह उसे लाल कर देती है।
(b) संतुलित अभिक्रिया: S + O₂ → SO₂।
10. लोहे को जंग से बचाने के दो तरीके बताइए।
उत्तर:
1. लोहे पर पेंट या तेल-चिकनाई लगाना।
2. जिंक की परत (गैल्वनाइजेशन) करना।
11. ऑक्सीजन के साथ संयोग होकर अधातु कैसा ऑक्साइड बनाते हैं?
उत्तर: अधातु, ऑक्सीजन के साथ मिलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं।
उदाहरण: C + O₂ → CO₂ (कार्बन डाइऑक्साइड)
12. कारण बताइए:
(a) टाइटेनियम, सोना एवं चाँदी अभिक्रियाशील नहीं होते, इसलिए आभूषण बनाने में उपयोगी हैं।
(b) सोडियम, पोटैशियम, लिथियम की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता के कारण इन्हें तेल में रखा जाता है।
(c) एलुमिनियम ऊपर से निष्क्रिय लेकिन अंदर सक्रिय होता है। ऊपर की परत भोजन से नहीं अभिक्रिया करती।
(d) सल्फ्यूरिक अम्ल का ऑक्साइडिक लोहा के साथ प्रतिक्रिया कर उसे घुलनशील बना देता है, इसलिए बर्तन काले नहीं होते।
13. नमक लोहे के बर्तनों में नींबू या इमली के रस से साफ करने पर असर क्यों दिखता है?
उत्तर: इमली या नींबू में एसिड होता है, जो आयरन के ऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर उसे साफ करता है।
14. रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में भिन्नता कीजिए।
उत्तर:
धातु:
1- इलेक्ट्रॉन खोते हैं।
2- ऑक्साइड क्षारीय होता है।
3- अम्ल से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं।
अधातु:
1- इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं।
2- ऑक्साइड अम्लीय होता है।
3- अम्ल से गैस नहीं बनाते।
15. एक महिला जंग लगा तांबे का लोटा साफ करने के लिए इमली के रस का उपयोग करती है। क्यों?
उत्तर: इमली के रस में उपस्थित अम्ल तांबे के ऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर उसे हटाकर लोटे को साफ और चमकदार बना देता है।
16. गर्म पानी के बर्तन बनाने में तांबे का उपयोग होता है, लेकिन इस्पात नहीं – क्यों?
उत्तर: तांबा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है और रासायनिक रूप से स्थिर भी है, इसलिए यह गर्म बर्तन के लिए उपयुक्त है।
जबकि इस्पात में लोहा होता है जो पानी और वायु से प्रतिक्रिया कर सकता है और जंग खा सकता है।
धातु एवं अधातु – महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)
1. कौन-सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है?
2. कौन-सी धातु चाकू से आसानी से काटी जा सकती है?
3. सबसे अच्छी विद्युत चालक धातु है–
4. नीचे दी गई धातुओं में से कौन अम्ल से हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती?
5. जंग से बचाने के लिए लोहे पर चढ़ाई जाने वाली धातु है–
6. कौन-सा यौगिक अम्लीय ऑक्साइड नहीं है?
7. धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं?
8. नीचे दिए गए में से कौन-सी अधातु है?
9. कौन-सा तत्व तन्य और आघातवर्ध्य दोनों है?
10. सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है?
11. चाँदी और सोना क्यों नहीं संक्षारित होते?
12. एलुमिनियम को अम्लीय भोजन पकाने के लिए क्यों उपयोग किया जा सकता है?
13. तांबे के बर्तन को इमली से क्यों साफ किया जाता है?
14. निम्न में से कौन-सा एक उपयोज्य ऑक्साइड है?
15. कौन-सी धातु अधातुओं से उत्पन्न अम्लीय गैसों से आसानी से प्रतिक्रिया कर लवण बनाती है?
16. निम्न में से कौन-सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलती है?
17. कौन-सा धातु गैस के रूप में पाया जाता है?
18. जंग लगने के लिए कौन-सी दो चीजें आवश्यक होती हैं?
19. पीतल किसका मिश्रधातु है?
20. कौन-सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है?
उत्तर कुंजी –
| प्रश्न क्रमांक | सही उत्तर |
|---|---|
| 1 | (b) पारा |
| 2 | (c) सोडियम |
| 3 | (c) चाँदी |
| 4 | (c) तांबा |
| 5 | (d) जिंक |
| 6 | (d) CaO |
| 7 | (b) क्षार |
| 8 | (b) सल्फर |
| 9 | (b) तांबा |
| 10 | (c) जल व वायु से प्रतिक्रिया रोकने के लिए |
| 11 | (c) ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं |
| 12 | (c) इसकी सतह पर ऑक्साइड परत होती है |
| 13 | (c) इमली में अम्ल होता है |
| 14 | (b) Na₂O |
| 15 | (c) कैल्सियम |
| 16 | (c) सोना |
| 17 | (c) कोई नहीं |
| 18 | (c) जल और वायु दोनों |
| 19 | (a) तांबा + जिंक |
| 20 | (c) पोटैशियम |
Class 10: विज्ञान
Chapter 1: रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण
Chapter 2: अम्ल, क्षार एवं लवण
NCERT BOOKS डाउनलोड करें।