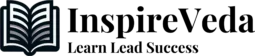मौलिक अधिकार, उनके अनुच्छेद, वाक् स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता
भारतीय संविधान की विशेषताएँ (Features of Indian Constitution)
भारत को संविधान में किन नामों से जाना गया?
– India, अर्थात् भारत। यह नाम भारत की आधुनिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है।
भारतीय संविधान की शासन प्रणाली:
भारत में संसदीय शासन है, जिसमें विधायिका कार्यपालिका को जवाबदेह बनाती है।
अध्यक्षात्मक प्रणाली का आधार: एकल कार्यपालिका
भारत और ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली में अंतर: भारत में न्यायिक समीक्षा है, जबकि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च होती है।
संविधान संघात्मक है: केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट वितरण इसका प्रमाण है।
मौलिक अधिकार
भारतीय संविधान के मूल्य:
- स्वतंत्रता
- लोकतंत्र
- समानता
- पंथनिरपेक्षता
- समाजवाद
- भातृत्व
- संप्रभुता
संविधान की आत्मा: नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार — ग्रेनविल ऑस्टिन
प्रमुख तथ्य (तालिका रूप में):
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| मूल संविधान में अनुच्छेद व अनुसूचियाँ | 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ |
| जन-गण-मन पहली बार कब गाया गया? | 1911, कलकत्ता अधिवेशन |
| राष्ट्रगान का मानक समय | 52 सेकंड |
| संविधान को “वकीलों का स्वर्ग” क्यों कहा जाता है? | जटिलता के कारण |
| कठोर+लचीले का संतुलन – किसका कथन? | के. सी. देवा |
डॉ. भीमराव अंबेडकर: “कोई भी संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले बुरे हों, तो वह बुरा सिद्ध होगा।”
महात्मा गांधी: स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को एक दल के रूप में भंग करने का सुझाव।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद: वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों तक स्थगित करने की बात संविधान सभा में रखी।
भारत के राष्ट्रीय प्रतीक
| प्रतीक | उत्तर |
|---|---|
| राष्ट्रीय पशु | बाघ |
| राष्ट्रीय पुष्प | कमल |
| राष्ट्रीय पक्षी | मोर |
| ध्वज के चक्र में तीलियाँ | 24 |
एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994): सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान को परिसंघात्मक माना।
सातवीं अनुसूची के प्रमुख विषय (Important Subjects of 7th Schedule)
भारतीय संविधान के अंतर्गत विभाजन प्रक्रिया तीन सूचियों के आधार पर की गई है:
- संघ सूची (Union List)
- राज्य सूची (State List)
- समवर्ती सूची (Concurrent List)
जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले समवर्ती सूची में शामिल हैं।
शिक्षा पहले राज्य सूची में थी, लेकिन 42वें संशोधन, 1976 के बाद समवर्ती सूची में डाल दी गई।
भूमि कर राज्य सूची का विषय है।
रेलवे संघ सूची का विषय है।
आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है।
कृषि राज्य सूची का विषय है।
पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भी राज्य सूची में आती है।
राज्यपाल तथा चुनाव संघ सूची के अंतर्गत आते हैं।
रक्त संक्रमण एवं अनुसंधान जैसे विषय समवर्ती सूची (अनुच्छेद 246, सूची-III) में शामिल हैं।
विवाह, तलाक, उत्तराधिकार एवं अंतरराज्यीय प्रवास समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं।
मौलिक अधिकार
तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय
| संघ सूची (Union List) | राज्य सूची (State List) | समवर्ती सूची (Concurrent List) |
|---|---|---|
| प्रतिरक्षा | पुलिस व्यवस्था | वन्य जीवों का संरक्षण |
| परमाणु मामले | बाजार एवं मेले | श्रम कानून |
| श्रेणीबद्ध रेल | शराब | समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय |
| मुद्राएँ/बैंक | मनोरंजन | स्वास्थ्य और औषधियाँ |
| विदेशी व्यापार | भू-राजस्व | आबादी नियंत्रण |
| लॉटरी | प्रति व्यक्ति कर | विवाह, तलाक, उत्तराधिकार |
वर्तमान स्थिति:
संघ सूची में 98 विषय, राज्य सूची में 59 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं।
भारतीय संविधान की उद्देशिका (Preamble of Indian Constitution)
प्रस्तावना (उद्देशिका)
हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:
- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
- विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
- प्रतिष्ठा और अवसर की समानता
- उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता
प्राप्त करने के लिए इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया?
– 13 दिसंबर, 1946
42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा तीन शब्द जोड़े गए:
- समाजवादी (Socialist)
- पंथनिरपेक्ष (Secular)
- अखंडता (Integrity)
उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है – ठाकुर केशव सिंह मामले एवं एम. मुनी द्वारा।
उद्देशिका से संबंधित प्रमुख तथ्य
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| प्रस्तावना को संविधान का भाग कब माना गया? | केशवानंद भारती केस, 1973 |
| राज्य का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? | समाजवाद |
| प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? | डॉ. धर्मवीर |
| प्रस्तावना को राजनीतिक ज्योतिष (Political Horoscope) किसने कहा? | के. एम. मुंशी |
“हम, भारत के लोग” (We, the People of India) से आरंभ होने का उद्देश्य: संविधान की प्रजातांत्रिक भावना और नागरिकों की संप्रभुता को दर्शाना।
उद्देशिका में कौन-कौन से तत्वों का उल्लेख है?
– मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व, और राष्ट्र की एकता व अखंडता के मूल्य।
बेरुबरी केस (1960) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस में इस पर पुनर्विचार किया गया।
एम. हिदायतुल्ला ने कहा: उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा को दर्शाती है।
संघ एवं राज्य क्षेत्र (Union and its Territories)
अनुच्छेद 1(3) के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:
- राज्य
- संघ राज्य क्षेत्र
- ऐसे अन्य क्षेत्र जो भारत में शामिल किए जाएँ
28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र वर्तमान में भारत में हैं।
31 अक्टूबर, 2019 को जम्मू-कश्मीर का विभाजन कर दो संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए – जम्मू-कश्मीर और लद्दाख।
राज्य का गठन संसद द्वारा किया जा सकता है।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया।
नए राज्यों के निर्माण हेतु संविधान में अनुच्छेद 2, 3 और 4 महत्वपूर्ण हैं।
विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा
| राज्य | वर्ष | राज्य | वर्ष |
|---|---|---|---|
| नागालैंड | 1963 | त्रिपुरा | 1972 |
| हिमाचल प्रदेश | 1971 | मणिपुर | 1972 |
| मेघालय | 1972 | मिजोरम | 1986 |
| सिक्किम | 1975 | गोवा | 1987 |
| अरुणाचल प्रदेश | 1987 | हरियाणा | 1966 |
मौलिक अधिकार
क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils)
| क्रम | परिषद् का नाम | मुख्यालय | सदस्य राज्य / संघ क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 1 | उत्तरी परिषद | नई दिल्ली | जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ |
| 2 | केंद्रीय परिषद | प्रयागराज | उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ |
| 3 | पूर्वी परिषद | कोलकाता | बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल |
| 4 | पश्चिमी परिषद | मुंबई | राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा-नगर हवेली एवं दमन-दीव |
| 5 | दक्षिणी परिषद | चेन्नई | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी |
वर्तमान स्थिति:
दिसंबर 1953 में फज़ल अली आयोग की सिफारिश पर तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था।
भारत के 28 राज्य व 8 केंद्रशासित प्रदेश
➤ भारत के राज्य
| क्रम | राज्य | राजधानी | भाषा | जिलों की संख्या | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | राष्ट्रीय क्षेत्रफल में % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राजस्थान | जयपुर | हिंदी | 50 | 3,42,239 | 10.41 |
| 2 | मध्य प्रदेश | भोपाल | हिंदी | 55 | 3,08,245 | 9.37 |
| 3 | महाराष्ट्र | मुंबई | मराठी | 36 | 3,07,713 | 9.36 |
| 4 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | हिंदी, उर्दू | 75 | 2,43,286 | 7.34 |
| 5 | गुजरात | गांधीनगर | गुजराती | 33 | 1,96,024 | 5.96 |
| 6 | कर्नाटक | बेंगलुरु | कन्नड़ | 31 | 1,91,791 | 5.83 |
| 7 | आंध्र प्रदेश | अमरावती | तेलुगु | 26 | 1,62,968 | 4.97 |
| 8 | ओडिशा | भुवनेश्वर | ओड़िया | 30 | 1,60,205 | 4.87 |
| 9 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | हिंदी | 33 | 1,35,191 | 4.11 |
| 10 | तमिलनाडु | चेन्नई | तमिल | 38 | 1,30,058 | 3.95 |
| 11 | बिहार | पटना | हिंदी | 38 | 94,163 | 2.87 |
| 12 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | बंगाली | 23 | 88,752 | 2.70 |
| 13 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | हिंदी | 26 | 83,743 | 2.55 |
| 14 | झारखंड | रांची | हिंदी | 24 | 79,714 | 2.42 |
| 15 | असम | दिसपुर | असमिया | 35 | 78,438 | 2.38 |
| 16 | हिमाचल प्रदेश | शिमला/धर्मशाला | हिंदी | 12 | 55,673 | 1.69 |
| 17 | उत्तराखंड | देहरादून/गैरसैंण | हिंदी, संस्कृत | 13 | 53,566 | 1.62 |
| 18 | पंजाब | चंडीगढ़ | पंजाबी | 23 | 50,362 | 1.53 |
| 19 | हरियाणा | चंडीगढ़ | हिंदी | 22 | 44,212 | 1.34 |
| 20 | सिक्किम | गंगटोक | नेपाली | 6 | 7,096 | 0.21 |
➤ केंद्रशासित प्रदेश
| क्रम | केंद्रशासित प्रदेश | राजधानी | जिलों की संख्या | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान व निकोबार | पोर्ट ब्लेयर | 3 | 8,249 |
| 2 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 1 | 114 |
| 3 | दादरा नगर हवेली व दमन दीव | दमन | 3 | 603 |
| 4 | दिल्ली | नई दिल्ली | 11 | 1,483 |
| 5 | लक्षद्वीप | कवरत्ती | 1 | 32 |
| 6 | पुदुचेरी | पुदुचेरी | 4 | 492 |
| 7 | जम्मू-कश्मीर | श्रीनगर/जम्मू | 22 | 54,624 |
| 8 | लद्दाख | लेह | 2 | 1,66,055 |
भारत का सबसे बड़ा जिला: कच्छ, गुजरात (45,652 वर्ग किमी)
भारत का सबसे छोटा जिला: माॅहे, पुदुचेरी (9 वर्ग किमी)
नागरिकता (Citizenship)
जन्म से, वंशानुक्रम द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, भूमि के अधिग्रहण द्वारा
भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है?
एकल नागरिकता (Single Citizenship)
संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद:
| अनुच्छेद | विषय-वस्तु |
|---|---|
| 5 | संविधान लागू होने के समय नागरिकता |
| 6 | भारत में प्रव्रजन द्वारा नागरिकता |
| 7 | पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले नागरिकों के अधिकार |
| 8 | विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता |
| 9 | भारत के बाहर स्वेच्छा से नागरिकता लेने पर नागरिकता समाप्त |
| 10 | भारत की संसद नागरिकता संबंधी नियम बना सकती है |
| 11 | संसद को नागरिकता से जुड़े नियम बनाने की शक्ति |
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) के अंतर्गत हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए, उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान है।
प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है।
NRI, PIO एवं OCI कार्डधारक में तुलना
| तुलना | अप्रवासी भारतीय (NRI) | भारतीय मूल का व्यक्ति (PIO) | विदेशी भारतीय नागरिक (OCI) |
|---|---|---|---|
| परिभाषा | भारतीय नागरिक जो सामान्यतः भारत से बाहर निवास करता है | पूर्वज भारतीय नागरिक हों या स्वयं भारत में जन्मा हो | जो विदेशी नागरिक भारतीय मूल का हो और भारत से संबंध रखता हो |
| नागरिकता की अधारिता | भारतीय नागरिक | नहीं | नहीं |
| प्राप्त होने की प्रक्रिया | भारत से बाहर निवास, पासपोर्ट द्वारा | कार्ड द्वारा विशेष स्थिति में | पंजीकरण द्वारा |
| वीजा आवश्यक | नहीं | हाँ | नहीं |
| मताधिकार | है | नहीं | नहीं |
नोट: एल. एम. सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस प्रति वर्ष 9 जनवरी को मनाने की अनुशंसा की थी।
मूल अधिकार (Fundamental Rights)
संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति न्यायालयों को प्रदान की गई है। (अनुच्छेद – 32, 226)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-13 ने संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध यदि कोई राज्य विधि बनाता है तो उसे शून्य घोषित किया जा सकता है।
समानता का अधिकार अनुच्छेद-14 से 18 में है।
केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार
- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद न करना (अनुच्छेद-15)
- लोक नियोजन के अवसर की समानता (अनुच्छेद-16)
- संगठन स्थापित करने की स्वतंत्रता, आंदोलन, रैली, सभा आदि (अनुच्छेद-19)
- अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद-29)
- शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार (अनुच्छेद-30)
मौलिक अधिकार
भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त मौलिक अधिकार
- विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण (अनुच्छेद-14)
- जीवन का अधिकार और वैयक्तिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद-21)
- कुछ आपराधिक निरोधक अधिकार (अनुच्छेद-22)
- धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद-25-28)
- नैतिक अपराधों के विरुद्ध संरक्षण (अनुच्छेद-20)
- संपत्ति अधिकार (पूर्व में अनुच्छेद 31, अब समाप्त)
संविधान में अस्पृश्यता किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्जित है?
अनुच्छेद-17 – अस्पृश्यता को समाप्त किया गया।
अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम, 1955 के अनुसार यह दंडनीय अपराध है।
उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में?
अनुच्छेद-18 – उपाधियों की समाप्ति
संविधान में मीडिया की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, परंतु अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इसे शामिल किया गया है।
नोट: आर्थिक समानता (Economic Equality) को भी समानता के मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है।
मौलिक अधिकारों के विस्तृत प्रावधान (Fundamental Rights – Article Wise)
अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएँ:
- वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता – अनुच्छेद 19(1)(a)
- शांतिपूर्ण, हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार – अनुच्छेद 19(1)(b)
- संगम, संघ, सहकारी समिति बनाने का अधिकार – अनुच्छेद 19(1)(c)
- भारत में अबाध संचरण का अधिकार – अनुच्छेद 19(1)(d)
- निवास व बसने का अधिकार – अनुच्छेद 19(1)(e)
- व्यवसाय या आजीविका का अधिकार – अनुच्छेद 19(1)(g)
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद:
- अनुच्छेद 20: दोषसिद्धि से संरक्षण व दोहरे दंड से मुक्ति।
- अनुच्छेद 20(C): स्वयं अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं।
- अनुच्छेद 21: जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
- अनुच्छेद 24: बच्चों के शोषण से संरक्षण।
- अनुच्छेद 25: हिन्दू शब्द में बौद्ध, जैन, सिख शामिल।
- अनुच्छेद 26: धार्मिक संस्थाओं की स्थापना व प्रबंधन का अधिकार।
- अनुच्छेद 30(1): अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार।
- अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचारों का अधिकार – डॉ. अंबेडकर के अनुसार यह संविधान की आत्मा है।
महत्वपूर्ण तथ्य:
- मौलिक अधिकारों का संरक्षक – न्यायपालिका
- Habeas Corpus याचिका – व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु
- केशवानंद भारती बनाम केरल वाद (1973) – संसद को संशोधन की सीमा तय हुई
- 44वां संविधान संशोधन (1978) – संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाया गया
- सूचना का अधिकार (RTI) – विधिक अधिकार (2005 से)
- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) हेतु – अनुच्छेद 15(6), 16(6)
- 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा – मूल अधिकार (अनु. 21A)
- राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित न होने वाला अधिकार – जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता
- बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम – 1976
मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण
| श्रेणी | अनुच्छेद |
|---|---|
| समानता का अधिकार | 14-18 |
| स्वतंत्रता का अधिकार | 19-22 |
| शोषण के विरुद्ध अधिकार | 23-24 |
| धर्म की स्वतंत्रता | 25-28 |
| संस्कृति और शिक्षा सम्बंधी अधिकार | 29-30 |
| संवैधानिक उपचारों का अधिकार | 32 |
संबंधित उपयोगी लिंक (Related Useful Links)
अधिक जानकारी के लिए निम्न स्रोतों को देखें